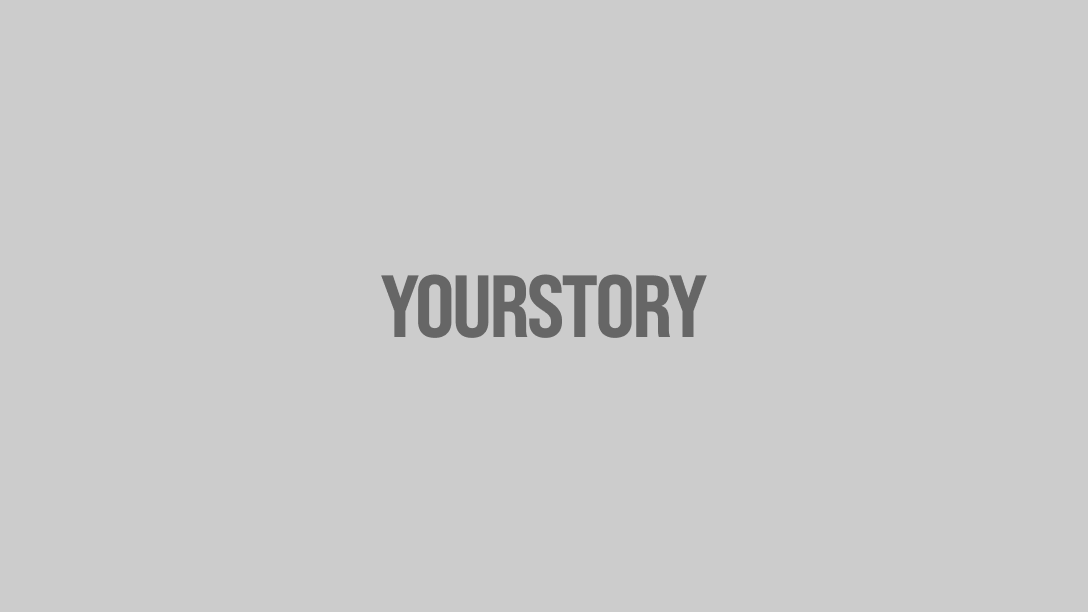32 किलोमीटर लम्बी चोरल नदी को पुनर्जीवित कर मालवा-निमाड इलाके में लोगों ने दी कई पीढ़ियों को नई ज़िंदगी
चोरल नदी को सामूहिक प्रयासों से पुनर्जीवित किया गया...
12 सौ फिट गहराई में जाकर काम करने की चुनौती को स्वीकारा...
9 करोड के प्रोजेक्ट को साढ़े पांच करोड रुपये में ही कर दिया पूरा...
साल भर पानी रहने से इलाके में हुई हरियाली....
मिलजुलकर किये प्रयास और हर चुनौती को स्वीकार करते हुऐ आगे बढते रहना एक ऐसा मंत्र है जिससे कोई भी लक्ष्य नामुमकिन की हद को पार कर जाता है। कहते हैं एक नदी को फिर से जीवित करना कई पीढ़ियों को नई ज़िंदगी देने के बराबर है। ऐसा ही एक प्रयास हुआ इंदौर के आस-पास के मालवा-निमाड इलाके में जहां लगभग मर चुकी एक नदी को सामूहिक प्रयासों ने जिंदा कर दिया। इतना ही नहीं ये सब हुआ लागत से आधे बजट में।
चोरल नदी वैसे तो एक बरसाती नदी है जो बरसात में इतने वेग से बहती है कि इसके पास जानें की सोचने से भी कोई सिहर उठे। मगर परेशानी ये थी कि पहाडों से आये पानी से अचानक नदी का वेग बढता था और बारिश थमते ही रुक जाता था। बरसात का पानी बमुश्किल दिसंबर तक भी नहीं ठहर पाता था। चोरल नदी यूं तो 35 किलोमीटर बाद नर्मदा में जाकर मिल जाती है। मगर इलाके के लिये इसको जिंदा करना बेहद जरुरी हो गया था। चोरल नदी की इस कहानी को समझने के लिये पहले इसकी भौगोलिक स्थिति को समझना जरुरी है। इंदौर से 55 किलोमीटर दूर जानापाव की पहाडी पर इसका उद्गम स्थल है। इंदौर मालवा इलाके में आता है जबकि मालवा से लगा निमाड इलाका इससे 13 सौ फिट नीचे है। यहीं मालवा के पहाडों से बरसात का पानी तेजी से नीचे पहुंचता है और नदी बनकर तेजी से बहता है। चोरल नदी निमाड इलाके में बडवाह के पास नर्मदा नदी में मिल जाती है। इस पूरे 35 किलोमीटर की नदी के आसपास 4 ग्राम पंचायतों के 17 गांव है। ये सभी गांव आदिवासी बाहुल्य गांव हैं जो पूरी तरह कृषि पर निर्भर हैं। नदी के किनारे के किसान गेहूं और सोयाबीन की फसल बोते थे। मगर नदी से दूर के किसानों के लिये तो पानी की भी समस्या थी। जीवन-यापन के लिये ये लकड़ी काटकर गुजारा करते थे। नदी किनारे के किसान भी साल में एक फसल लेने के बाद हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाया करते थे।

इस नदी को पूरे सालभर तक लबालब रखने और जिंदा करने के लिये कागजी योजना शुरु हुई। खर्च का बजट बना लगभग 9 करोड से ऊपर का। पहली चुनौती तो इसको आधे बजट तक लाने की हुई। भारत सरकार के भूमि एंव जल संसाधन विभाग मध्यप्रदेश सरकार के पंचायत एव ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के तहत इसकी योजना तैयार हुई। जमीन पर काम शुरु करने के साथ सबसे चुनौती नदी के रास्ते में आ रही रुकावटों को हटाना था, जिससे नदी इधर-उधर घुसने की बजाय अपने रास्ते पर ही चले। नदी के सबसे पहले नीचे गिरने की जगह पर गांव था केकरिया डाबरी। ये गांव 12 सौ फिट नीचे था। 8 परिवारों की आबादी वाला ये गांव आम लोगों की पहुंच से दूर था। जहां जाने के लिये कोई सडक नहीं थी। नीचे जाना का रास्ता दुर्गम है। पहाडों से पत्थरों को पकड कर नीचे जाना पडता था। तो जाहिर है कि वहां तक निर्माण सामग्री और मशीनें कैसे पहुंचाई जाये। उसके लिये सबसे पहले एक कच्चा रास्ता बनाकर इस कार्यक्रम की नींव रखी गई। बैलगाडी, ट्रैक्टर और खच्चर के सहारे धीरे-धीरे सामान नीचे पहुंचाकर जमा करना शुरु किया। इस प्रोजेक्ट की लागत कम करने के लिये नीचे बसे गांव के लोगो को साथ में लिया गया, जिन्होने प्रशासन और इलाके में काम करने आई संस्था की मदद की। पहाडों पर तेजी से वन-विभाग की मदद से कंटूर टैंचेस, बोल्डर चेक और खेतों पर मेड़ बंदी की गई। चोरल से मिलने वाली छोटी नदी और नालों का भी ट्रीटमेंट करके उनके रास्ते की रुकावटें हटाई गईं। इन कार्यों से मिट्टी की कटाई रोकने में सौ फीसदी सफलता मिल गई।

रास्ते में आने वाले 2 दर्जन बंद पड़े नालों और दो नदियों को ढूंढकर वापस जीवित करने की कवायद शुरु हुई। इतने नीचे जेसीबी या फिर कोई आधुनिक मशीन जा नहीं सकती थी। इसका हल भी ढूंढा गया 500 साल पुरानी तकनीकि से। नालों के शुरु होने की जगह से आदिवासी मजदूरों की टोली हाथ में गेंती, फावडा लेकर निकल पडी। नालों के रास्ते में जो भी पत्थर चट्टान या रुकावटे दिखीं उनको तोडते हुऐ चलते गये। देखते-देखते पहाडों से पानी ले जाकर नदी में छोडने वाले नाले एक बार फिर अपने साठ साल पुराने स्वरुप में लौट आये। चोरल नदी में 6 और सहायक नदी में 2 स्टॉप डैम बनाये गये। 2011 में शुरु हुऐ इस प्रोजेक्ट में जी तोड़ मेहनत के बाद इस साल जो रिजल्ट सामने आया वो वाकई हैरान कर देने वाला था। दिसम्बर तक सूख जाने वाली नदी फरवरी में भी लबालब भरी हुई है।

हर साल इस वक्त तक सूख चुका इलाका आज पानी से लबरेज है। जिसे देखकर किसानों में बेहद उत्साह है। इस मिशन में काम करने वाली संस्था नागरथ चेरीटेबल ट्रस्ट के प्रभारी सुरेश एमजी ने योरस्टोरी को बताया,
"लगातार 5 साल तक कड़ी मशक्कत रहने के बाद आज वो दिन आ गया जिसका सभी को इंतजार था। हमने प्रोजेक्ट 5 करोड 45 लाख रुपये में कम्पलीट कर दिया। ये सब हुआ टीम वर्क के चलते। इलाके के आदिवासी, जिला प्रशासन, वन-विभाग सभी ने इस प्रोजेक्ट पर खुद को झोंक दिया। उसी का नतीजा अब सबके सामने है।"

इंदौर कलेक्टर पी नरहरी के मुताबिक,
"चुनौती बहुत बडी थी। 12 सौ फीट नीचे जाकर काम करना आसान नहीं था। जरुरत थी सबको साथ लेकर चलनें की। हर कदम पर एक नई चुनौती खडी हो जाती थी, मगर हम बिना देर करे तत्काल बैठकर उसका समाधान खोजते जा रहे थे। आज इलाके में पानी हो गया है। अब किसानों को लाभ वाली खेती की तरफ मोड़ना है। जिसके लिये हमनें उद्धानिकी विभाग के साथ मिलकर किसानों को फूलों की खेती शुरु करवाई है। सिंहस्थ 2016 के लिए अप्रेल से किसानों का उत्पादन उज्जैन पहुंचने लगेगा। और आर्थिक तौर पर उनकी जिंदगी में एक नया दौर शुरु हो जायेगा।"
दो चरणों में चलने वाले इस प्रोजेक्ट का फिलहाल पहला ही चरण पूरा हुआ है। जबकि दूसरे चरण में तीन और बडे स्टॉप डैम बनाये जाना बाकी हैं।